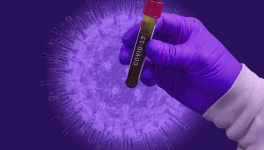भारतीय पूंजीवाद के लिए कृषि आज भी 'खपाऊ' क्षेत्र बनी हुई है
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिना किसी योजना के चार घंटे की मोहलत पर तीन सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा ने अचानक लाखों प्रवासी श्रमिकों के जिस संकट को सामने ला दिया है, उससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू उजागर होता है। उजागर होने वाले इस पहलू में यह सच्चाई भी है कि गांव, अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और संयुक्त-परिवार प्रणाली के साथ उन करोड़ों शहरी कामगारों के लिए आज भी आधार बने हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी पूंजीवाद के तहत उतार-चढ़ाव से भरी हुई है।
जब उनकी आय अचानक शून्य हो गयी और वे बेघर बना दिये गये, और सचमुच सड़कों के हवाले कर दिये गये, तो उनके दिमाग़ को हिला देने वाला विचार आया, वह विचार था-उनकी गांव वापसी का, भले ही इसके लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना था। पत्रकारों से बातचीत में कई लोगों ने कहा कि गांव में अपने घर वापस आने पर उन्हें कम से कम रबी की फ़सल के लिए फ़सल-श्रमिकों के तौर पर कुछ रोज़गार तो मिलेगा। संक्षेप में कहा जाये,तो गांव और कृषि क्षेत्र अब भी भारतीय पूंजीवाद के लिए "खपाऊ क्षेत्र" बने हुए हैं।
अपने प्रवक्ताओं की तरफ़ से प्रचारित इस मिथक के बिल्कुल उलट, पूंजीवाद उन सभी छोटे-छोटे उत्पादकों को खपा नहीं पाता है,जिन्हें वह विस्थापित करता है। पूंजी संचय एक हद तक श्रम-बचत करने वाले उन तकनीकी बदालावों के साथ होता है, जो उन सभी श्रमिकबलों को इस व्यवस्था में खप जाने से रोकता है,जिनकी संख्या में प्राकृतिक बढ़ोत्तरी होती रहती है और जिन्हें एक साथ विस्थापित कर दिया जाता है। यही कारण है कि जहां ये विस्थापित होते हैं,उसे हमेशा एक "खपाऊ क्षेत्र" के वजूद की तरह देखा जाता है, यानी एक ऐसी जगह,जहां सभी दुखी, व्यथित आबादी इकट्ठा हो जाती है।
महानगरीय पूंजीवाद में यह "खपाऊ क्षेत्र" गोरी बस्तियों वाला वह समशीतोष्ण क्षेत्र था, जहां यूरोप से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इन नये क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी वहां के मूल निवासियों,अमेरिंडियों को अपने भूमि क्षेत्र से विस्थापित करके जीवन का एक माकूल मानक हासिल करने में कामयाब रहे।
ग़रीबी और औद्योगिक क्रांति पर चली पारंपरिक अंग्रेज़ी बहस में तो एरिक हॉब्सबॉम जैसे लोगों ने भी यह तर्क दिया था कि औद्योगिक क्रांति के बाद ग़रीबी बढ़ गयी थी, उन्होंने इस बात को क़ुबूल किया था कि 1820 के दशक में इंग्लैंड में चीज़ों में सुधार होना शुरू हो गया था, और इस हक़ीक़त के लिए उस पूंजी संचय को ज़िम्मेदार ठहराया था,जिसने आख़िरकार अभाव और ग़रीबी में सेंध लगा दी थी।
हालांकि, असलियत में यह पूंजी संचय था ही नहीं, बल्कि पलायन था, जिसमें नेपोलियन से जुड़े युद्धों के ख़त्म हो जाने के बाद तेज़ी आयी थी, और इससे बहुत फर्क पड़ा था। यूरोपीय पूंजीवाद का यह "खपाऊ क्षेत्र",जो कि आख़िरकार इतना परेशान करने वाला तो नहीं था, लेकिन इसे "नई दुनिया" कहा गया, यानी समशीतोष्ण बस्ती वाला इलाक़ा।
लेकिन,भारत जैसे उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में, जहां महानगरीय पूंजीवाद के हमले से विस्थापित हुए लोगों के लिए पलयान की कोई और गुंजाइश थी ही नहीं, ऐसे में उनके “खप जाने वाला क्षेत्र” वह घरेलू कृषि क्षेत्र था, जहां महानगर में पूंजी के संचय के साथ-साथ संकट और दुःख,दोनों बढ़ते रहे।
आज़ादी के बाद, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर राज्य के नियंत्रण में उस समय फ़र्क़ आया, जब प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। हालांकि इसके लाभ हुए,लेकिन उस लाभ का बटवारा ग्रामीण वर्गों के बीच ग़ैर-बराबरी स्तर पर किया गया; और कृषि के बाहर रोज़गार के अवसरों में बढ़ोत्तरी तो हुई,लेकिन यह बढ़ोत्तरी श्रमिकों की बढ़ोत्तरी की दर से थोड़ा ही ज़्यादा थी।
ऊपर बताये गये दोनों घटनाक्रम के कारण कृषि के भीतर जीवन स्तर में मामूली सुधार हुआ, जो कि औपनिवेशिक शासन की पिछली आधी सदी में होने वाली घटनाओं के उलट था। लेकिन, अब हम फिर से नवउदारवादी पूंजीवाद के साथ हैं, जब "खपाऊ क्षेत्र" में रहने वाले लोग अपने जीवन स्तर में हो रही गिरावट का गवाह बन रहे हैं।
भारत के "आर्थिक महाशक्ति" या "5-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था" के तौर पर उभरने को लेकर की जाने वाली बड़ी-पड़ी बातें भी इस बात को नहीं छुपा सकती है कि किसानी कृषि आज भी एक "खपाऊ क्षेत्र" बनी हुई है,जो पूंजी संचय की प्रक्रिया से फ़ायदा उठाने के बजाय समय के साथ बढ़ते संकट का गवाह बन रहा है, श्रमिकों को उससे दूर कर रहा है। नवउदारवाद के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था की कथित "कामयाबी" के पीछे, क्या इस "खपाऊ क्षेत्र" के भीतर का बढ़ता संकट तो नहीं है, जिसकी विडंबना यह है कि देश का बहुसंख्यक कार्य बल यहीं केंद्रित है और जैसा कि हम नीचे इस बात को रखेंगे कि किस तरह यह संपूर्ण भारतीय श्रम-बल के हालात को तय करता है।।
इस सच्चाई का एक निहितार्थ भी और वह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एक "खपाऊ क्षेत्र" के रूप में कार्य करती है। संगठित श्रमिकों सहित शहरी श्रमिकों की सौदेबाज़ी की क्षमता,कृषि पर आधारित कामकाज़ी आबादी की प्रति व्यक्ति आय के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें वे ज़मींदार, पूंजीवादी किसान और समृद्ध किसानों शामिल नहीं हैं,जो कृषि से बाहर भी अलग-अलग काम को अंजाम देते हैं।
यहां तक कि भारत के संगठित श्रमिक भी अपनी ग्रामीण जड़ों से पूरी तरह से कटे हुए नहीं होते हैं, और जिन क्षेत्रों में वे कार्यरत होते हैं, वहां लगातार हड़ताल पर जाने की उनकी क्षमता अक्सर उनकी जड़ों से मिलने वाली मदद के स्तर पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाये, तो यह उन भौतिक स्थितियों पर निर्भर करती है, जो उनके घर वापसी पर भी बनी रहती हैं, जिसके लिए हमने कृषि में काम करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को सूचकांक के तौर पर अपनाया है।
इसलिए, हम समकालिक रूप से आगे-पीछे गतिशील मज़दूरों, किसानों और खेतिहर मज़दूरों वाली इस अर्थव्यवस्था में सभी श्रमजीवियों की ज़िंदगी के हालात की कल्पना कर सकते हैं। इस समकालिक गतिशीलता के लिए यह सक्रियता या तो कृषि विकास की ओर से आ सकती है या फिर शहरी रोज़गार में होने वाली बढ़ोत्तरी की तरफ़ से आ सकती है, और ये दोनों,बारी-बारी से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक कृषि आय जैसे ही कृषि क्षेत्र को मिलने वाले सरकारी समर्थन से हाथ खींच लेने के कारण गिर जाती है, वैसे ही यह अर्थव्यवस्था में कामकाजी लोगों के पूरे समुदाय के हालात में नीचे की ओर होने वाली गति का कारण बन जाता है; ठीक इसी तरह, रोज़गार देने वाली शहरी अर्थव्यवस्था की क्षमता जैसे ही श्रमबल के विकास की प्राकृतिक दर से नीचे आ जाती है, तो वैसे ही पूरी कामकाजी आबादी नीचे की ओर पलायन कर जाती है। जैसा कि पहले ही इस बात का ज़िक्र किया जा चुका है कि ये दोनों कारक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं; और नवउदारवादी शक्ति के तहत दोनों कारक संचालित होते हैं।
लेकिन,ऐसा भी नहीं है। नवउदारवाद के तहत एक ऐसी बढ़ती हुई गतिशीलता भी होती है, जो काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर के बदतर करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाती रहती है।।
आइए, हम यह मान लेते हैं कि रोज़गार शुरू करने के लिए ग़ैर-कृषि क्षेत्र में मौजूदा विकास दर की क्षमता,कार्य-बल के विकास की प्राकृतिक दर से नीचे आ जाती है। इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि यह क्षमता न सिर्फ़ विकास दर पर निर्भर करती है, बल्कि इसके साथ आने वाली तकनीकी प्रगति की दर पर भी निर्भर करती है।
अगर विकास से पैदा होने वाले रोज़गार के अवसरों में प्राकृतिक श्रमबल की बढ़ोत्तरी को नहीं खपाया जा सकता है, तो कामकाजी आबादी के जीवन के हालात उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है। इसका आवश्यक रूप से मतलब अर्थव्यवस्था में शोषण की दर में बढ़ोत्तरी से है, जो कि पारंपरिक राष्ट्रीय आय लेखांकन के सिलसिले में कुल जीडीपी के आर्थिक अधिशेष की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी के तौर पर ख़ुद को सामने रखता है।
हालांकि, श्रम की बचत करने वाली तकनीकी प्रगति की दर, कुल उत्पादन में आर्थिक अधिशेष की हिस्सेदारी पर निर्भर करती है, क्योंकि अधिशेष पर निर्भर रहने वाले वालों की मांग का स्वरूप महानगरीय जीवनशैली के क़रीब होता है। शुरुआत में इस तरह की जीवनशैलियां न सिर्फ़ बहुत कम रोज़गार प्रधान वाली होती है, बल्कि ये आगे मशीनरी के इस्तेमाल में होने वाली तेज़ी से होने वाले बदलाव और इससे रोज़गार में आने वाली कमी की दिशा के अधीन भी होती है। यही वजह है कि शोषण की दर में प्रारंभिक बढ़ोत्तरी के साथ-साथ इसमें शोषण की दर में और ज़्यादा बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति होती है।
हम यहां काम कर रहे लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर रहे हैं।शोषण की इस दर में होने वाली लगातार बढ़ोत्तरी का मतलब उनके संपूर्ण जीवन स्तर का बदतर होना है, जिसका मतलब उनकी संपूर्ण ग़रीबी की सीमा में बढ़ोत्तरी होने से है।
यह बिल्कुल वैसा ही है,जैसा कि भारत में हो रहा है, जहां जनसंख्या का वह अनुपात भारत में ग़रीबी को परिभाषित करने के लिए आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मानक पोषण सम्बन्धी मानदंडों तक नहीं पहुंच सका है, जिसमें नवउदारवाद काल के दौरान बढ़ोत्तरी हुई है। यहां याद दिलाना ज़रूरी है कि ये मानदंड, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2,200 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2,100 कैलोरी का है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक़, ग्रामीण भारत में इस मानक स्तर तक पहुंच बनाने में असमर्थ रहे लोगों का अनुपात 1993-94 में 58% से बढ़कर 2011-12 में 68% हो गया था। इसी तरह, शहरी भारत में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2,100 कैलोरी का उपयोग करने में असमर्थ रहे लोगों का यह अनुपात ऊपर ज़िक्र किये गये इन दो अवधियों के बीच 57% से बढ़कर 65% हो गया।
COVID-19 महामारी से ग़रीबी की हालत और भी बदतर होगी, क्योंकि इससे शहरी बेरोज़गारी में भारी बढ़ोत्तरी होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसा पहले ही हो चुका है। बल्कि,जिस तंत्र के ज़रिये ग़रीबी में यह बढ़ोत्तरी पूरे क्षेत्र में हुई है, वह सही मायने में लॉकडाउन के दौरान बेपर्द हो गयी है, यानी, जो लोग शहरी क्षेत्र में बेसहारा हो गये हैं,वे ही बड़े पैमाने पर गांव की ओर पलायन करने लगे हैं।
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।