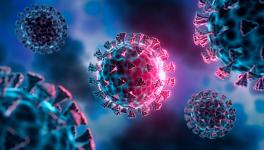कोविड-19: संवैधानिक सबक़ और शासन व्यवस्था
कोविड-19 की मौजूदा लहर की जिस तबाही से भारत इस समय गुज़र रहा है और जिसने हमारी शासन प्रणाली की जिन कमियों को बेपर्दा कर दिया है, उन्हीं कमियों का विश्लेषण स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की संवैधानिक गारंटी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में वित्तीय असंतुलन और इस संकट के प्रबंधन की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के ख़ास नज़रिये से अखिल वी.मेनन और रस्सल जनार्दन कर रहे हैं। वे अपने इस लेख के ज़रिये हमारे संस्थागत लचीलेपन को मज़बूत बनाने का सुझाव भी दे रहे हैं।
इस समय हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह अपने देश के इतिहास की अभूतपूर्व चुनौती है। इस महामारी ने बेशुमार क़ीमती ज़िंदगियां छीन ली हैं और हमारे देश को एक-एक सांस से जूझने के लिए विवश कर दिया है। जैसे ही यह महामारी थम जायेगी, यह अपने पीछे हमें एक ऐसे देश के तौर पर छोड़ देगी, जिसे हो सकता है कि पहचान पाना भी मुश्किल हो, क्योंकि तब यहां एक गहरी ग़ैर-बराबरी अपनी जगह बना चुकी होगी। इसके अलावा, इस महामारी ने हमारे अधिकारों को लेकर न्याय-व्यवस्था और संस्थागत लचीलापन के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिये हैं।
ऐसे में वायरस के विनाशकारी प्रभाव से अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करते हुए इन बड़े-बड़े मुद्दों का पता लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
संवैधानिक गारंटी के तौर पर स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार हमारी स्वास्थ्य सेवा से जुडा बुनियादी ढांचा रहा है। महामारी ने भौतिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की कमी जैसे व्यवस्था से जुड़े पहले से मौजूद मुद्दों पर हमारे ध्यान को टिका दिया है।जहां हमसे कहीं ज़्यादा आबादी वाले चीन ने बड़े पैमाने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करके अपने बुनियादी ढांचे को मज़बूत कर लिया है, वहीं हमारी सरकार इस ज़रूरत को उस स्तर पर पूरा करने में सक्षम नहीं है।
जिस वक़्त हम कोविड से हो रही मौत में लगातार इज़ाफ़ा होते देख रहे हैं और ठीक उसी वक़्त हमारे कई अस्पताल ऑक्सीजन की ख़तरनाक कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यह संवैधानिक सवाल सामने आ खड़ा होता कि क्या हम जीवन के अधिकार का इस्तेमाल सही मायने में कर पा रहे हैं ?
इस अधिकार के दायरे में आने वाले अधिकारों की एक श्रृंखला भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। वर्ष 1989 में पंडित परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1989 एससीआर (3) 997) के मामले में उस ऐतिहासिक फ़ैसले के ज़रिये जीवन के अधिकार के एक अटूट हिस्से के तौर पर स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की अवधारणा को जोड़ा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को अनुच्छेद 21 के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी थी।
तब से शीर्ष अदालत ने एक मज़बूत स्वास्थ्य देखभाल की न्याय व्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996 SCC (4) 37) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संविधान एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना करता है, जिसमें सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराना है।
भारत में एक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की यह कोशिश उस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समझौते (10 अप्रैल 1979 को भारत द्वारा मंज़ूर) के अनुच्छेद 2 (1) के तहत परिकल्पित दायित्व के अनुरूप भी है, जिसमें शामिल देशों का कर्तव्य है कि वे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को धीरे-धीरे अमली जामा पहनाना सुनिश्चित करें।
हालांकि, इस तरह के नज़रिये के आलोचकों का कहना है कि देश की वित्तीय अक्षमता की वजह से पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार जैसे इन आर्थिक अधिकारों पर अमल कर पाना मुश्किल है। न्यायपालिका ने ख़ुद इस मुद्दे को पंजाब बनाम राम लुभाया बग्गा ((1998) 4 एससीसी 117) के मामले में संबोधित करने की कोशिश की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को मुकम्मल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश असीमित संसाधनों की आपूर्ति वाला देश नहीं होता, और जिस स्तर तक यह अधिकार हासिल किया जा सकता है, वह स्तर राज्य की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है;इसलिए, राज्य मशीनरी को किसी ऐसी सुविधा मुहैया नहीं करा पाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसकी वित्तीय क्षमता से बाहर हो।
भारत में डॉक्टर-मरीज़ का अनुपात 1:1, 456 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1: 1000 के अनुपात से 30 प्रतिशत कम है। इसके अलावा, भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, इसके सकल घरेलू उत्पाद का 1.29% है, जो ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका) देशों में सबसे कम है। हालांकि, पिछले दशक में कई देशों की सरकारों की तरफ़ से स्वास्थ्य पर किये जाने वाले सरकारी ख़र्च में गिरावट आयी है।
मामलों की मौजूदा स्थिति हमारे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की भयाभह तस्वीर को सामने लाती है। इस लिहाज़ से एक ज़रूरी सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 की सीमा का विस्तार करने के लिहाज़ से कोई वास्तविक प्रगति की है ?
सुप्रीम कोर्ट की असमर्थता उसके अधिकारों के क्षेत्राधिकार का विस्तार को ज़मीन पर उतारने के लिहाज़ से न्यूनतम आर्थिक निवेश सुनिश्चित करने के सिलसिले में उसके ख़ुद के फ़ैसलों के समय-समय पर किये जाने वाले मूल्यांकन की कमी में निहित है। इसलिए, इसकी कई शानदार घोषणायें महज़ काग़ज़ी बनी हुई हैं, और इसकी चर्चा देश के लॉ कॉलेजों की चार दीवारों तक सीमित है। ऐसे में किसी को हैरानी हो सकती है कि न्यायपालिका अपने फ़ैसलों को ज़मीन पर भला किस तरह उतार सकती है।
न्यायपालिका के लिए एक तरीक़ा तो यह हो सकता है कि वह ख़ास तौर पर संविधान के भाग III के विषय में अपनी न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिहाज़ से सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों को प्रभावी रूप से चिह्नित करने के लिए ‘न्यायिक प्रभाव आकलन’ के बड़े बैनर तले कार्यपालिका के साथ समय-समय पर बातचीत शुरू करे। इससे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में बुनियादी न्यूनतम वित्तीय निवेश सुनिश्चित करने में कार्यपालिका की भूमिका के आसपास की चर्चाओं को मुख्यधारा की चर्चा बनाया जा सकता है।
कल्याणकारी राज्य को लेकर हमारी तलाश के सिलसिले में न्यायपालिका की ऐसी सक्रिय भूमिका ज़रूरी है।
वित्तीय संघवाद की ज़रूरत
हालांकि, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की समस्या का हल महज़ न्यायपालिका के ज़रिये नहीं पाया जा सकता। इसके लिए विधायी और नीतिगत स्तरों पर किसी आमूल-चूल बदलाव की ज़रूरत है। भारतीय संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार (सूची II के अनुसार, संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 6) पर डालता है। हालांकि, असली सवाल तो यही है कि क्या इस तरह की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया गया है ? स्वास्थ्य सेवा पर ख़र्च करने के लिहाज़ से कई राज्य सरकारें जिन संकटों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए हमारे देश के राजकोषीय संघवाद की त्रुटियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
संघ और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार के इन दोनों स्तरों के बीच गहरा असंतुलन मौजूद है। इस असंतुलन के लिए संविधान के तहत केन्द्र को मिली कराधान की व्यापक शक्ति के मुक़ाबले राज्यों को मिली अपेक्षाकृत कम शक्ति को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदारीकरण की व्यवस्था ने राज्यों के बीच की असमानताओं को और गहरा कर दिया है, इस तरह, असंतुलन का विस्तार और हुआ है।इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा विदेशी उधारों पर संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा तय की गयी सीमायें, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM अधिनियम) द्वारा लगाये गये प्रतिबंध, अन्य चीज़ों के अलावे वस्तु और सेवा कर जैसे सुधार ने राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का काम किया है।
राज्यों को हासिल वित्तीय स्वायत्तता की कमी की वजह से कई राज्यों में बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं हो पाया है। महाद्वीप के आकार वाले किसी देश में सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के किसी भी प्रयास को जड़ों से शुरू करना चाहिए, और राज्य सरकारों को स्थानीय स्व-शासन के ज़रिये इन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए सर्वोत्तम रूप से संसाधनों से लैस होना चाहिए।
यह महामारी हमारे राजकोषीय ढांचे के मौजूदा ढांचे को फिर से निर्माण किये जाने की ज़रूरत की ओर इशारा करती है। बिना किसी शर्त के उधार लेने की सीमाओं को हटाने और एफआरबीएम अधिनियम में ढील देने जैसे कुछ ऐसे क़दम हैं, जिन्हें छोटे और मध्यम अवधि में उठाया जा सकता है।
लम्बे समय में राज्यों को अपने ख़ुद के संसाधन के सृजित किये जाने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, करों के लगाये जाने के उनके अधिकारों और केन्द्र-राज्य के बीच करों के बंटवारे के दावे सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये संवैधानिक दायित्वों में भी प्रतिबिंबित होने चाहिए।
प्रशासनिक संकट के समय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
स्वास्थ्य का अधिकार कुछ समय तक तो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन, हमारी तत्काल प्राथमिकता महामारी का प्रभावी प्रबंधन है।
सरकार की तरफ़ से अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जिस तरह की चिंताजनक और जटिल स्थिति है, उसमें संवैधानिक अदालतें कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकती हैं, और ऐसे हालात में कार्यपालिका की समझ-बूझ पर भरोसा करना सबसे अच्छा होता है।
बेशक, यह यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वह अपनी समझ-बूझ कार्यपालिका पर थोपे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को उस प्रवासी संकट के मद्देनज़र की गयी अपनी टिप्पणी की रौशनी में एक मूक दर्शक के रूप में नहीं बने रहना चाहिए, जो पिछले साल भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देखा गया था। लिहाज़ा, महामारी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती प्रतिक्रिया उसकी भूमिका को सही नहीं ठहराती है।
इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई होई कोर्टों ने इस संकट के समय में बेहतर प्रदर्शन किया है। मसलन, अपने-अपने राज्यों में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश के हाई कोर्टों के हालिया हस्तक्षेप तारीफ़ के क़ाबिल हैं।
कोविड-19 की दूसरी लहर ने सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर लगे लांछन से छुटकारा पाने का एक और मौक़ा दे दिया है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट का हालिया हस्तक्षेप इस संकट काल में एक मिसाल क़ायम करने की उम्मीद दिखाता है। शीर्ष अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को अपनी टीकाकरण नीति के औचित्य और इसके ऑक्सीजन के राज्यवार आवंटन के सिलसिले में बार-बार सवाल किया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का यह संवाद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ़ से जारी 27 अप्रैल 2021 के आदेश में साफ़-साफ़ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप संकट के समय कार्यपालिका के कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिहाज़ से अहमियत रखता है।
सुप्रीम कोर्ट इस अभूतपूर्व संकट के समय में हमारे लोकतांत्रिक अधिकार के सामूहिक इस्तेमाल के एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, अच्छी तरह से काम करने वाली संसद और एक संगठित विपक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट को अपनी भूमिका को अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन मज़बूत करना चाहिए, ताकि इस संकट के समय संवैधानिकता के सिद्धांत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
इस महामारी ने हमारी शासन प्रणाली की कमियों की श्रृंखला को बेरहमी से उजागर कर दिया है, और ऐसे में हमारे मूल अधिकार को असरदार बनाया जा सके, इसके लिए सुधार की ज़रूरत है। जन-जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिहाज़ से हमारा संस्थागत लचीलापन अहम साबित होगा। संकट कई मोर्चों पर हुई गड़बड़ियों के सुधार करने और संवैधानिक लोकाचार में निहित राष्ट्र के निर्माण का अवसर प्रस्तुत करता है।
जैसा कि हारुकी मुराकामी ने अपनी किताब, 'काफ़्का ऑन द शोर' में लिखा है:
“एक बार जब तूफ़ान थम जायेगा, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप इस तूफ़ान को कैसे झेल गये, आप कैसे बचे रह गये। आप यह भी तय नहीं कर पायेंगे कि क्या तूफ़ान सही में थम गया है भी कि नहीं। लेकिन, एक बात तो तय है। जब आप तूफ़ान से बाहर निकल आयेंगे, तो आप वही शख़्स नहीं होंगे, जो तूफ़ान से गुज़रकर आया है। इस तूफ़ान के बारे में यही सच है।”
हमें उम्मीद है कि एक राष्ट्र के रूप में हम संगठित और प्रभावी संस्थानों के साथ इस महामारी से बाहर निकल आयेंगे, और नये सिरे से सभी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकारों की गारंटी से सुसज्जित एक बराबरी वाले समाज की ओर अपना क़दम बढ़ायेंगे।
यह लेख मूल रूप से द लीफ़लेट में प्रकाशित हुआ था।
(अखिल वी. मेनन और रसल जनार्दन ए, दोनों ही केरल स्थित अधिवक्ता हैं, और कोच्चि के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस लीगल स्टडीज़ से स्नातक हैं। इनके व्यक्त विचार निजी हैं।)
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
https://www.newsclick.in/COVID-19-Lessons-Constitution-Governance
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।