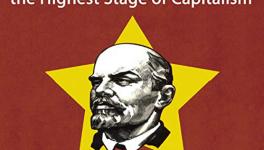तीसरी दुनिया का विदेशी ऋण संकट सरल अर्थशास्त्र की रौशनी में

भारत और तीसरी दुनिया के अन्य देश, साम्राज्यवादी ताकतों के साथ अपने जी-20 में शामिल होने होने को नैतिक रूप से तभी उचित ठहरा सकते हैं, जब वे जी-20 की बैठकों में समग्रता में तीसरी दुनिया की साझा तथा ज्वलंत समस्याएं उठा पा रहे हों।
तीसरी दुनिया की विदेशी ऋण समस्या
शायद, आज ऐसी समस्याओं में सबसे ज्वलंत समस्या तो विदेशी ऋण की ही है, जिसे नवउदारवादी पूंजीवाद के वर्तमान संकट ने उभारकर सामने ला दिया है। जी-20 के वर्तमान अध्यक्ष तथा उसके अगले शिखर सम्मेलन के मेजबान के नाते भारत को तीसरी दुनिया के लिए विदेशी ऋण से राहत के मुद्दे को, इस सम्मेलन में उठाना चाहिए। इस मुद्दे पर काफी भ्रम बना हुआ है, जबकि सरल अर्थशास्त्र को टटोलने से ही यह मुद्दा स्पष्ट हो जाना चाहिए। आइए, देखें कि कैसे सरल अर्थशास्त्र से यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है।
तीसरी दुनिया के विदेशी ऋण के संबंध में आम धारणा यह है कि इन देशों को ये ऋण देने के लिए, विकसित देशों ने अपने घरेलू उपभोग या निवेश में से कटौतियां कर के ये साधन निकाले हैं। बेशक, तीसरी दुनिया के देशों द्वारा लिए गए ऋण वित्तीय संस्थाओं से आए हैं, लेकिन इस तरह के ऋण इन देशों के चालू खाता घाटों की भरपाई करते हैं। इन देशों के चालू खाता घाटे से फालतू जितना भी ऋण लिया जाएगा, वह सीधे-सीधे इन देशों के विदेशी मुद्रा संचित कोष में जुड़ जाएगा और इसलिए, यह उनके शुद्ध ऋण का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बेशक, अगर किसी खास साल में घाटे की भरपाई करने के लिए कुछ शुद्ध ऋण लिया जाता है, तो बाद में इस तरह का घाटा नहीं रहने के बावजूद, शुद्ध ऋण का परिमाण तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि इस ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगायी जा रही होगी। लेकिन, सारा का सारा प्राथमिक शुद्ध ऋण तो चालू घाटों की भरपाई करने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए ही लिया जा रहा होगा। आम धारणा के अनुसार, इस तरह के संसाधनों का ऋण के रूप में दिया जाना, ऋणदाता देशों द्वारा अपने संसाधनों का बलिदान किए जाने को ही दिखाता है और इसलिए, आगे चलकर उन्हें अपनी इस कुर्बानी के बदले में समुचित भुगतान मिलना ही चाहिए।
विदेशी ऋणदाता देशों के कुर्बानी देने का भ्रम
बहरहाल, सरल अर्थशास्त्र पर नजर डालने से भी साफ हो जाता है कि यह समूची धारणा ही पूरी तरह से गलत है। जब किसी माल की आपूर्ति की सापेक्षता में मांग में कमी होती है, तीन प्रकार के समायोजन संभव होते हैं। संबंधित माल के दाम घट सकते हैं; संबंधित माल की ज्यादा इन्वेंट्रियां खड़ी हो सकती हैं या फिर उसके उत्पाद में ही कमी हो सकती है। अब विनिर्मित मालों (तथा सेवाओं) की कीमतें आम तौर पर कुलीनतंत्रीय उत्पादकों द्वारा तय की जाती हैं और इसलिए कीमतें प्राय: गिरती नहीं हैं। हां, कभी एक तात्कालिक पैंतरे के तौर पर ऐसा किया जा रहा हो तो बात दूसरी है। इसी प्रकार इन्वेंट्रियों में बढ़ोतरी को भी जल्द ही निकाल दिया जाता है और इस तरह बढ़ी हुई इन्वेंट्रियों को ज्यादा समय तक बनाकर नहीं रखा जाता है। इसलिए, मांग में गिरावट से, उत्पाद में ही कटौती होती है। और अगर अर्थव्यवस्था को समग्रता में लिया जाए तो, यानी सभी मालों को मिलाकर देखा जाए तो (अगर समग्रता में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पहलू में आम तौर पर विनिर्मित माल व सेवाएं ही आते हैं, जैसाकि विकसित पूंजीवादी देशों के मामले में होता है) तो, किसी भी समय विशेष पर उसका जितना उत्पाद होता है, वह उतना इसीलिए होता है कि उसकी मांग न इससे ज्यादा होती है और न कम। इसीलिए, पूंजीवाद एक मांग-बाधित व्यवस्था होता है: पूंजीवाद के अंतर्गत किसी खास समय पर उत्पाद तथा रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त सकल मांग नहीं होती है।
अब विकसित पूंजीवादी देशों के साथ लेन-देन में तीसरी दुनिया के देशों के चालू खाता घाटे, विकसित देशों की चालू व्यापार बचत के सिवा और कुछ नहीं होते हैं और यह चालू व्यापार बचत, उनकी सकल मांग का ही एक घटक होती है। अगर यह चालू व्यापार बचत नहीं होती, तो उतनी मात्रा में उत्पाद पैदा ही नहीं हुआ होता। इसलिए, तीसरी दुनिया के देश, विकसित देशों से जो वास्तविक सेवाएं तथा माल ऋण के तौर पर लेते हैं, वे तो पैदा ही इस तरह का ऋण लिए जाने के चलते ही हो पाते हैं। इसलिए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा तीसरी दुनिया के देशों को ऋण देने के लिए, अपने घरेलू उपभोग या निवेश में कटौतियां कर के कोई कुर्बानी दी जा रही होती है।
ऋणदाता को मांग में बढ़ोतरी से लाभ ही लाभ
लेकिन, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मान लीजिए कि तीसरी दुनिया के किसी देश के साथ लेन-देन में, विकसित देशों की बचत 100 डॉलर की है, जो विकसित देशों द्वारा उसे ऋण के तौर पर दे दी जाती है। यह 100 डॉलर की राशि, विकसित देश के घरेलू निवेश के वित्त पोषण के निवेश के ऊपर से, उसकी अतिरिक्त बचत बन जाती है। अगर संबंधित विकसित देश/ देशों का बचत अनुपात (यानी राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में बचतों का हिस्सा) 25 फीसद हो, तो 100 डॉलर की इस अतिरिक्त बचत को पैदा करने के लिए, उनकी आय में 400 डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि विकसित दुनिया के उपभोग में, 300 डॉलर की बढ़ोतरी हुई होगी (यानी 400-100=300)। इसलिए, विकसित दुनिया द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उसके द्वारा अपने उपभोग में किसी तरह की कटौती किए जाने की बात तो दूर रही, वहां इस ऋण की राशि से तीन गुना ज्यादा अतिरिक्त उपभोग पैदा कर रहा होता है।
इस तरह, तीसरी दुनिया को ऋण देने में विकसित दुनिया कोई कुर्बानी नहीं दे रही होती है। उल्टे संबंधित ऋण के चलते, उसका घरेलू उपभोग बढ़ता ही है, जो उस ऋण के न दिए जाने की स्थिति में नहीं हुआ होता। उसके कुल उत्पाद में इतनी बढ़ोतरी होती है, जो उसके उपभोग में बढ़ोतरी तथा उसके द्वारा दिए गए ऋण के योग के बराबर होती है और उसके रोजगार में भी उसी हद तक बढ़ोतरी होती है। संक्षेप में यह कि ऋण देने का, विकसित दुनिया की कुल आय पर बहुगुणनकारी प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव, अगर विकसित दुनिया का बचत अनुपात 25 फीसद हो, तो 4 के अंक के बराबर होगा। संक्षेप में बहुगुणनकारी प्रभाव, बचत अनुपात के साथ चलता है।
सचाई पर पर्दा डालने का खेल
यह सब एकदम सरल अर्थशास्त्र का मामला है। (स्कूली पाठ्यपुस्तकों में भी यह सब पढ़ाया जाता था, हालांकि मैं कह नहीं सकता कि निर्बुद्घिकरण के लिए अपने मोह के चलते, भाजपा सरकार ने इसे पाठ्यपुस्तकों से निकलवा नहीं दिया होगा।) इस सबका अर्थ यह है कि अगर, तीसरी दुनिया पर, विकसित दुनिया का जितना भी ऋण है, वह पूरा का पूरा भी माफ कर दिया जाता है, तब भी विकसित दुनिया उस स्थिति के मुकाबले रत्तीभर नुकसान में नहीं होगी, जब उक्त ऋण दिया गया था और वास्तव में उस स्थिति के मुकाबले फायदे में ही होगी क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में उसके उपभोग तथा रोजगार में बढ़ोतरी हुई होगी।
ऋण देने के ठीक इसी निहितार्थ के चलते ब्रेटन वुड्स संस्थाओं द्वारा, विकसित दुनिया के वित्तीय स्वार्थों द्वारा और अर्थशास्त्र के पेशे द्वारा जिसने अपने इस अनुशासन को ऐसी चीज में बदल दिया है जिसे मार्क्स ने ‘‘भोंडा अर्थवाद’’ कहा होता, इस सचाई को ढांपने की ही कोशिश की जाती है। वे न सिर्फ वास्तविक संसाधनों के सिलसिले में ‘बलिदान’ दिए जाने के आख्यान को प्रचारित करते हैं (जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं अपरिहार्य रूप से आपूर्ति-बाधित होती हों) बल्कि वे वित्तीय संसाधनों की एक दुर्लभता का भी आविष्कार कर लेते हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि ऋण देने के लिए उपलब्ध फंड तो किसी भी समय पर सीमित ही होते हैं!
केन्स से ब्रांट आयोग तक
जाने-माने अंग्रेज अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड केन्स ने महामंदी के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की थी, जो उस समय पर पहली नजर में अजीब सी लगती थी। उन्होंने कहा था कि अगर सार्वजनिक काम की परियोजनाओं में मजदूरों को सिर्फ जमीन पर गड्ढे खोदने और उन्हें भरने के ही काम में लगा दिया जाता है, तब भी इससे समाज अंतत: फायदे में ही रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर 100 डॉलर ऐसी ‘पूरी तरह से निरर्थक’ परियोजनाओं पर ही लगाए जाते हैं, तब भी उनसे 300 डॉलर का अतिरिक्त उपभोग पैदा होगा और उससे जुड़कर उसी हिसाब से अतिरिक्त रोजगार पैदा हो रहा होगा। और यह समाज को पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचा रहा होगा। अब तीसरी दुनिया को दिया गया 100 डॉलर के ऋण को अगर माफ कर दिया जाता है, तो यह ठीक उसी प्रकार के निरर्थक खर्च का मामला बन जाएगा, जैसा निरर्थक खर्च जमीन में गड्ढे कराना तथा उन्हें भरवाना होता। इसका अर्थ यह है कि निरर्थक खर्च के बावजूद, ऋण देने वाला खुद फायदे में ही रहेगा।
प्रसंगत: बता दें कि ब्रांट आयोग की इस सिफारिश के पीछे भी यही सोच थी कि विकसित देशों को अपनी हर वर्ष अपने जीडीपी का एक फीसद, अल्प विकसित देशों के लिए अनुदान देने के वास्ते अलग कर के रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्नत देशों को रत्तीभर नुकसान नहीं होगा क्योंकि वे तो वैसे भी मांग-बाधित व्यवस्थाएं ही चला रहे होते हैं। उल्टे, इससे इन देशों का संकीर्ण आर्थिक फायदे के लिहाज से भी लाभ ही हो रहा होगा और यह होगा इन अनुदानों के ‘बहुगुणनकारी प्रभावों’ के चलते।
कुछ भिन्न प्रकृति के ऋण
बहरहाल, यहां तक हम तीसरी दुनिया के विदेशी ऋणों को, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की उन पर देनदारियों के रूप में ही देखते आ रहे थे। जाहिर है कि सचाई इससे भिन्न है। इसमें कुछ ऋण मिसाल के तौर पर चीन का भी होगा और आमतौर पर परोक्ष रूप से तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं का भी ऋण होगा, जिसका लेन-देन विकसित दुनिया के बैंकों के माध्यम से होता है। इन ऋणदाताओं के मामले में पीछे हमने जो चर्चा की है वह प्रासंगिक नहीं होगी क्योंकि विकसित देशों की विनिर्माण आधारिक अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न, न तो चीन को मांग बाधित अर्थव्यवस्था माना जा सकता है और न तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं को। इसका अर्थ यह हुआ कि तीसरी दुनिया के कर्जदार देशों को, इन अग्रणी देशों के साथ अपनी अलग से ही व्यवस्थाएं निर्मित करनी चाहिए, ताकि उनके साथ विकसित दुनिया की वित्तीय संस्थाओं को माध्यम बनाए बिना, सीधे अपने संबंध विकसित कर सकें और उनसे ऋण राहत भी हासिल कर सकें। अब जबकि विश्व अर्थव्यवस्था पर विकसित पूंजीवादी दुनिया का दबदबा कमजोर हो रहा है, अलग से ऐसी स्वतंत्र व्यवस्थाएं खड़ी करने की संभावनाएं आज कहीं बढ़ गयी हैं।
तीसरी दुनिया के कर्जदार देशों के हितों के तकाजे
बहरहाल, जहां तक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का सवाल है, चूंकि यह आम धारणा पूरी तरह से गलत ही है कि उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों को ऋण देने में, अपनी ओर से कोई ‘कुर्बानियां’ दी हैं, तीसरी दुनिया के कर्जदार देशों को ऋणों के मामले में भुगतान आदि की ऐसी शर्तें तक करनी चाहिए जो उनकी आर्थिक जरूरतों के अनुरूप हों, न कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बीच में पड़ कर तय कराए गए ‘बचाव पैकेजों’ के साथ खुद को बांधना चाहिए। इस तरह के पैकेज तो कर्जदार देशों में जीवन स्तर को तथा इसलिए मांग को सिकोड़ने के जरिए, ऋण लेने वाली अर्थव्यवस्थाओं को निचोड़कर ही, उनमें से ऋण संबंधी भुगतानों के लिए संसाधन निकालने का काम करते हैं और इस तरह बुनियादी तौर पर ऋणदाताओं के ही स्वार्थों की हिफाजत करते हैं।
बेशक, अकेले-अकेले तो किसी भी कर्जदार देश में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि वह विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उलझ सके और ऋण संबंधी पुनर्भुगतानों तथा ब्याज के भुगतानों के लिए, अपनी ही शर्तें तक कर सके। लेकिन, एक समूह के रूप में तो ये कर्ज लेने वाले देश ऐसा कर ही सकते हैं। मिसाल के तौर पर वे यह शर्त लगा सकते हैं कि ऋण संबंधी भुगतानों के लिए समय-सीमाएं लागू कराए जाने के बजाए, उन्हें इसका मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपनी निर्यात आय का एक निश्चित हिस्सा हर साल इस काम के लिए निकालें, जैसा कि पेरू के पूर्व-प्रधानमंत्री, एलन गार्सिया ने अपने देश की अर्थव्यवस्था के मामले में एक जमाने में किया भी था। और इसके साथ ही साथ वे यह भी मांग कर सकते हैं कि खुद कर्ज की राशि को भी, काफी घटाकर लगाया जाना चाहिए।
जाहिर है कि इस सबके लिए पहले से ही ऋण लेने वाले देशों के बीच बातचीत का होना जरूरी है और इसके बाद ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले देशों के बीच वार्ता की जरूरत होगी। भारत जैसे देशों को, जो जी-20 के सदस्य हैं, ऐसी वार्ता की व्यवस्था कराने के लिए पहल करनी चाहिए।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।