महाराष्ट्र सरकार का एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर नया प्रस्ताव : असमंजस में ज़मीनी कार्यकर्ता
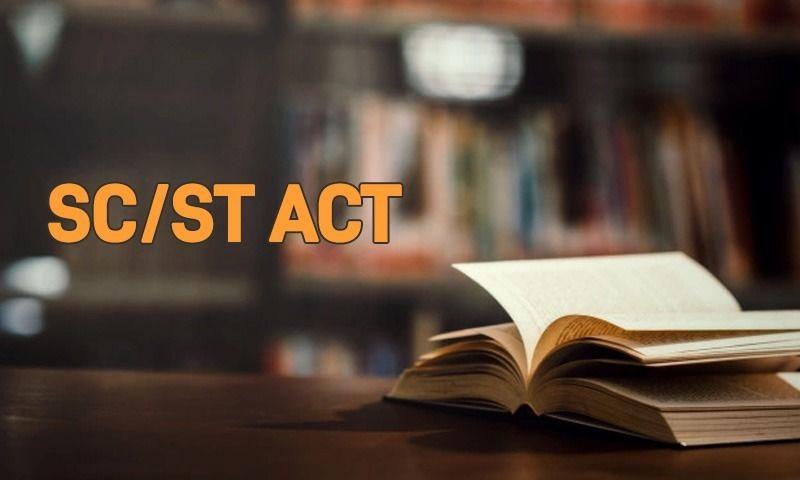
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 10 जनवरी 2022 को राज्य के DGP को भेजे गए पत्र के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर असहज माहौल पैदा हो गया। पत्र में महाराष्ट्र शासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक और सहायक पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारियों को स्थानांतरित करने की योजना का खुलासा किया है। राज्य के कानून एवं न्यायपालिका विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। माहौल के असहज होने का मूल कारण यह है कि, वर्तमान में पीओए अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत 1995 में बने केंद्रीय नियम के रूल 7 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार के मामलों की जांच डीवाईएसपी रैंक से नीचे के स्तर के अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सरकार के अकस्मात प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है।
राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव से सम्बंधित न ही कोई घोषणा की है और न ही प्रस्ताव के ऊपर कोई टिप्पणी दी है; परन्तु एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस फोर्स में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या और जिम्मेदारियों का अनुपात काफी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्याचार के मामलों की जांच निपटाने में जरूरत से ज्यादा समय लगता है। वहीं कुछ दलित कार्यकर्ताओं और वकीलों के एक तबके ने राज्य के इस प्रस्ताव की निंदा की है तथा इसे दलित और आदिवासी आबादी के अधिकारों के विपरीत कहा है।
दिल्ली की एक जानी मानी वकील ने राज्य की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा है कि “राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए निर्मित केंद्रीय कानून को कमजोर करने की कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 23 के तहत संसद के दोनों सदनों की मंज़ूरी के बाद पारित किए गए थे”।
हालांकि, इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को गैरकानूनी कहना अधिनियम की गलत समझ पर आधारित है तथा बिना पुख्ता जानकारी ऐसे विचार व्यक्त करना भ्रामक हो सकता है। क्योंकि वास्तव में अधिनियम की धारा 9 राज्य सरकार को यह ताकत देती है कि आवश्यकता अनुसार वे किसी भी अधिकारी को गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियां प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।
वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ़ बिहार बनाम अनिल कुमार एंड अदर्स नामक केस में बिहार सरकार के ऐसे ही एक प्रस्ताव को कानूनी दायरे के अंदर बताया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम' की धारा 23 और धारा 9 के दायरे भिन्न हैं; जहाँ धारा 23 के तहत केंद्र सरकार के पास निहित नियम बनाने की शक्ति के राष्ट्रीय स्तर की है, वहीं धारा 9 एक राज्य विशिष्ट शक्ति है जिसका उपयोग संबंधित राज्य अपने राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। इसलिए राज्यों द्वारा, धारा 9 के तहत किये गए किसी भी प्रयोग की वैद्यता की जांच संबंधित राज्य में स्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में एससी / एसटी समुदायों के साथ काम करने वाले संगठनों के समूह कारवाँ के मुख्य सलाहकार एवं दलित अत्याचार मामलों के कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट अंबादास बनसोडे ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “शिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं का कानूनी रूप से गलत एवं भ्रामक टिप्पणियां देना निराशाजनक है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जांच के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने के लिए राज्यों को अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति दी गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के अवैध होने का सवाल ही नहीं उठता। इन आधारहीन मतों को नज़रअंदाज़ करके यह समझने की आवश्यकता है कि इस बदलाव से अत्याचार अधिनियम के तहत हो रही जांचों के तरीके में किस प्रकार के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं”।
प्रस्ताव को लेकर कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का विचार है कि जहाँ निचले रैंक के अधिकारी जनता में सुलभ होते हैं वहीं उच्च रैंक के अधिकारी जैसे डीवाईएसपी का कार्यालय ब्लॉक स्तर पर होता है, इसी कारण ज्यादातर पीड़ितों का उच्च अधिकारी के कार्यालय तक जाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। साथ ही उनका उच्च पद, पीड़ितों और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की समझौता वार्ता की क्षमता भी कम करता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिनके अनुसार इस कदम से केंद्रीय नियम, 1995 द्वारा बनाये गए जांच के मज़बूत सिस्टम के कमजोर पड़ने की आशंका है। उनका कहना है कि निचली रैंक के पुलिस अधिकारी पक्षपात और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और बहुत ही आसानी से उच्च जाति के दबाव में आ सकते हैं। इन्ही अड़चनों की वजह से दलित अत्याचार के केसों की गलत जांच होने की संभावना है।
दोनों ही विचार पुलिस बल के असंतोषजनक, पक्षपाती और असंवेदनशील रवैये का परिणाम हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का पुलिस से असंतोष निराधार नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को दबंग तथा उच्च जातियों का साथ देकर अत्याचार के केसों को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्रों का सहारा लेते देखा गया है। इस समय यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या जांच का दायरा बढ़ाने से तथा पहले से स्थापित पुलिस सिस्टम के निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच की शक्ति देने से दलित अत्याचार से संबंधित जांच में कोई व्यवस्थागत बदलाव की गुंजाइश है?
ज़मीनी हकीकत तथा जानकारों की बातचीत से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल जांच के दायरे के विस्तार से मदद नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, 2008 में बिहार सरकार द्वारा किये गए जांच शक्तियों के विस्तार के बाद भी राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक कुल 49,008 मामलों में से, बिहार में केवल 12 दोष सिद्ध हुए, यह स्थिति 2007 से भी दयनीय है क्योंकि 2007 में कुल 7417 मामलों में से 175 मामलों में दोषियों को सज़ा हुयी थी।
पुणे में स्थित एक नॉन प्रॉफिट संस्था माणुसकी की कार्यकर्ता एडवोकेट प्रतिभा कहती हैं कि “हम इस बात की सराहना करते हैं कि सरकार जांच में देरी को लेकर चिंतित है, लेकिन केवल जांच के ढांचे में निचले रैंक के अधिकारियों को शामिल करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अत्याचार निवारण अधिनियम में विशेष न्यायालयों, विशेष अधिवक्ताओं और यहां तक कि विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। क्या ऐसे में सरकार को अधिनियम के तहत हुए अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई का गठन नहीं करना चाहिए ? अधिनियम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों या अधिकृत अधिकारियों को न्याय की एक मजबूत भावना और जाति आधारित अपराधों को समझने की क्षमता प्रदान करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज, मजबूत, विशिष्ट और केंद्रित बनाना है। समय-समय पर राज्यों ने उचित जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने विशेष रूप से अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस स्टेशन (एससी / एसटी कल्याण पुलिस स्टेशन) नियुक्त किए हैं। जांच के ढाँचे को मज़बूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के लिए भी यह उचित समय है”।
फिर समस्या की जड़ कहाँ है? जानकारों की बातचीत और जमीनी हकीकत से यह बात तो स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण सामाजिक कानून के संबंध में अलग-अलग राय और अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से जिन चुनौतियों का सामना किया है उनके मद्देनज़र सबसे पहले इस बात पर रोशनी डालने की जरूरत है कि अत्याचार अधिनियम के गठन के पीछे संसद की क्या मंशा थी। इस बात में कोई संकोच नहीं है कि यह अधिनियम वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हो रहे भेदभाव और सामाजिक अक्षमताओं को मिटाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसीलिए राज्य सरकार को अधिनियम के तहत कोई भी कदम उठाने से पूर्व इसके उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। साथ ही, अधिनियम को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए सरकार को सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ काम करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के नीतिगत बदलाव से पहले पड़ितों के साथ जुड़ने और उनके अनुभवों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि न्याय मिलने में हो रही कठिनाईयों और जातिगत अत्याचारों की निरंतरता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को चिह्नित किया जा सके।
[लेखिका अभिलाषा यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन (YHRD) से जुड़ी वकील हैं, YHRD वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा रिसर्च से जुड़े लोगों का नेटवर्क है। लेखक संघर्ष आप्टे पुणे में स्थित माणुसकी नामक संस्था में रिसर्चर हैं और KARVA के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।]
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।























